मानव जीवन में शिक्षा सबसे बड़ी सम्पति है, इसी बात को समझते हुए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया है।
शिक्षा किसी भी बच्चे के जीवन में परिवर्तक का काम करती है, देश के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुँचने के बाद ही यह देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलेगा।
देश में बढ़ती महँगाई और निजी स्कूलों की फीस एवं अन्य खर्चे शिक्षा में बाधक है। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षा को लेकर एक अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 पारित किया है।
इस लेख के अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिनियम 2009 से जुड़े जरुरी बिंदुओं की जानकारी मिलेगी।
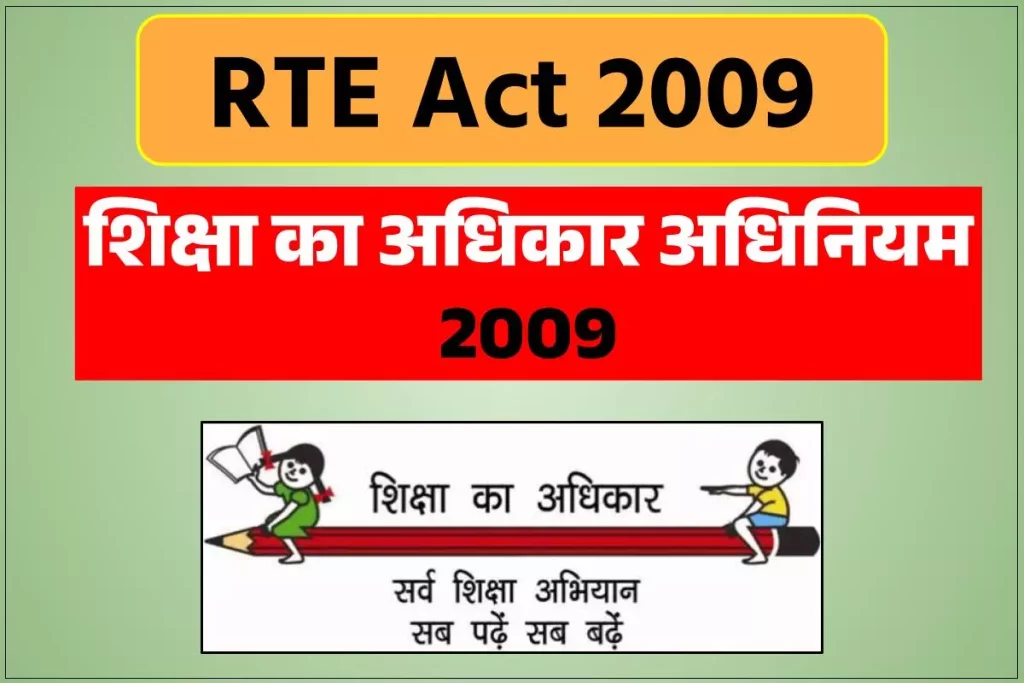
शिक्षा का अधिकार – RTE Act 2009
देश के बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च संपत्ति माने जाते है, क्योकि यह बहुत सी संभावनाओं से परिपूर्ण मानव संसाधन है। वर्तमान समय में शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देने का कार्य करती है।
शिक्षा का अधिकार 2009 सभी को शिक्षा देने के सपने को साकार करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो भारत में शिक्षा एक सांविधानिक अधिकार था, जोकि प्रारम्भ में एक मौलिक अधिकार भी है।
देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत देश की शिक्षा नीति को निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को दस वर्षों की समयसीमा के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु सभी बच्चों की शिक्षा को शुरू से 14 वर्ष की उम्र तक पूरी करवानी होती है।
आरटीई एक्ट 2009 में शिक्षा अभियान में निम्न है –
- बच्चों की पहचान।
- शिक्षा से सम्बंधित औपचारिक मूल्यांकन।
- जरुरत के अनुसार सही शिक्षा व्यवस्था देना।
- व्यक्तिगत योग्यता के अनुरूप शिक्षा योजना को बनाना।
- मददगार एवं दूसरे उपकरणों की व्यवस्था देना।
- टीचर्स ट्रेनिंग।
- बाहरी अध्यापक की मदद।
- वस्तु से जुड़े अवरोधों को हटवाना।
- शोध, देखरेख एवं मूलयांकन करना।
- दिव्यांश कन्याओं पर खास ध्यान।
RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ
संविधान के 86 वें संशोधन में अधिनियम 2002 में 21(A) को जोड़ा गया, जिसमें ये वर्णित है। कि प्रदेश को विधि बनाकर 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने के लिए अपबंद करेगा।
इसके बाद संसद में इस अधिकार को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया।
यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वित हुआ था, अधिनियम में 7 अध्याय एवं 38 खंड है। केंद्र सरकार पीएम छात्रवृति योजना से बच्चों को 2,500 से 3,000 रुपए की मदद दे रही है।
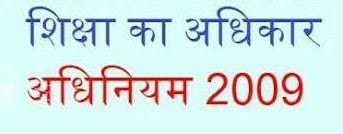
आरटीई एक्ट 2009 अधिनियम की विशेषताएँ
- एक्ट में देश के 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को “निःशुल्क एवं अनिवार्य” प्राथमिक शिक्षा देने के प्रावधान है।
- ये सुविधा 6 से 14 साल उम्र के अशिक्षित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए है।
- ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का काम स्कूली प्रबंधन समिति एवं स्थानीय निकायों का है।
- प्रबंधन समिति एवं क्षेत्रीय निकाय के द्वारा बच्चों के चिन्हीकरण का काम घर-घर सर्वे से होगा।
- ऐसे सर्वेक्षण द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों की खोज करने में सरलता होगी।
- सभी प्राइवेट स्कूलों की 2 प्रतिशत सीट आरटीई एक्ट 2009 में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी।
- इन छात्रों को वही शुल्क देना है, जो कि राजकीय स्कूल के छात्र देते है।
- 6 से 14 साल की आयु वर्ग के सभी छात्र और छात्राओं को ये अधिकार है, कि वे अपनी शुरूवाती शिक्षा अपने नजदीक के किसी स्कूल से निःशुल्क पा सकते है।
- अगर किसी विद्यार्थी का चयन विद्यालय में 6 वर्ष की उम्र में नहीं हो पाया तो वह बाद में भी अपनी आयु के अनुसार प्रवेश ले सकता है।
- अगर विद्यार्थी 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुवाती शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है, तो इसके बाद भी वह निःशुल्क शिक्षा पाने योग्य रहेगा।
- अगर किसी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है, या फिर किसी वजह से कोई विद्यार्थी अपना विद्यालय बदलने की इच्छा रखता है, तो उसे स्कूल बदलने का अधिकार मिलेगा।
- अधिनियम के घोषित होने के तीन वर्षों में ही प्रदेश सरकार एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को नजदीक में विद्यालय बनाना है। और जिस स्थान पर विद्यालय नहीं है, वहाँ विद्यालय भी स्थापित करना होगा।
- देश की केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के खर्चे की गणना बनाएगी, और प्रदेश सरकारों को जरुरी तकनीक मदद एवं साधन प्रदान करके विद्यालय स्थापित करने में योगदान करेगी।
- प्रदेश सरकार 6 से 14 साल के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में एडमिशन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह देखेगी कि कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव ना होने पाए।
- राज्य सरकार इस अभियान में विद्यालय बिल्डिंग, अध्यापक और शिक्षण सामग्री इत्यादि बेसिक जरूरतों को सुनिश्चित करेगी।
- किसी विद्यालय द्वारा एक्ट का पालन न होने पर अथवा अधिक शुल्क माँगने पर शुल्क का 10 गुना भुगतान करना होगा और स्कूल की मान्यता भी रद्द होगी।
आरटीई अधिनियम के उद्देश्य
- अधिनियम देश के सभी राज्यों के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियो को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
- स्थानीय स्कूल में 6 साल के सभी बच्चों का नामांकन जरुरी होगा।
- अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को ‘प्राइमरी शिक्षा’ की तरह परिभाषित करता है।
- अपनी प्राइमरी शिक्षा के पूरी होने से पूर्व किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में नहीं रोका जाएगा।
- किसी भी विधार्थी को कक्षा 8 तक अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा।
- पहली से आठवीं तक की शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थी को ‘प्रमाण-पत्र’ भी मिलेगा।
- 6 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद भी नामांकन ना होने पर बच्चे को उचित कक्षा में नामांकन मिलेगा।
- किसी भी राजकीय अध्यापक को अपना निजी शिक्षण संस्थान एवं निजी अध्यापन के कार्य की अनुमति नहीं होगी।
- नियमानुसार स्कूल में शिक्षक-छात्र का अनुपात 1:30 रहेगा अर्थात एक शिक्षक पर 30 छात्र।
- स्कूल में छात्रों एवं छात्राओं के लिए भिन्न-भिन्न टायलेट की सुविधा होगी।
- जरुरी प्रमाण-पत्रों के कारण से किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा।
- विद्यालय में नामांकन हेतु किसी भी बच्चे का एडमिशन टेस्ट नहीं होगा।
आरटीई एक्ट में एडमिशन लेने की प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने क्षेत्र में आईटीई कोटे वाले स्कूल को खोजे इसके लिए ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- कोटे के अंतर्गत स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सरकारी पोर्टल पर लॉगिन होकर फॉर्म भरकर प्रिंट कर लें।
- हर राज्य के लिए एक अलग आईटीई पोर्टल बनाया गया है।
- अपने चुने हुए स्कूल में आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ फॉर्म जमा कर दें।
- सरकारी स्कूल में प्रवेश की गारंटी रहती है, और निजी स्कूल में कानून 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश मिलेगा।
- सरकारी स्कूल में टेस्ट नहीं होगा, जबकि निजी स्कूल में टेस्ट होने पर इसके मानदण्ड संचालक मंडल तय करेगा।
- फॉर्म जमा होने के बाद प्रवेश मिलने पर निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगा।
- प्रवेश के समय बच्चे को निःशुल्क नोटबुक, किताबें एवं स्टेशनरी मिलेगी।
- दस्तावेज़ ना होने अथवा इनमें कमी होने पर भी प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश मिलेगा।
- बच्चे अपने क्षेत्र के अधिकतम 5 ही स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराएँ
- धारा 1 – इसमें संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार एवं लागू होने की तारीख के विषय में उल्लेख मिलता है।
- धारा 2 – अधिनियम से जुडी शब्दावली के मतलब मिलेंगे।
- धारा 3 – प्रदेश के सभी 6 से 14 साल की उम्र के विद्यार्थियों को नज़दीक के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक शुरूआती शिक्षा मिलेगी।
- धारा 4 – आयु के अनुसार एडमिशन, खास ट्रेनिंग अथवा मदद प्रदान करना जिससे निर्धारित समय सीमा में दूसरे बच्चों के समान में लाया जा सके। ऐसे 14 वर्षों के बाद भी प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार मिल सके।
- धारा 5 – विद्यालय से स्थानांतरण का अधिकार, प्रदेश के अंदर या फिर बाहर के स्कूल में प्रवेश का अधिकार, माँगने पर शीध्र प्रमाण-पत्र मिलना, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने में न ही देरी और प्रमाण-पत्र ना होने पर एडमिशन से न ही इंकार होगा। ऐसा होने पर सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
- धारा 6 – अधिनियम के बनने के 6 महीने बाद स्कूल ना होने पर स्कूल की व्यवस्था करना।
- धारा 7 –
- केंद्र और प्रदेश सरकारें पैसे की उपलब्धता तय करेगी।
- केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने के खर्च का आंकलन का कार्य करेगी।
- केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से सलाह एवं सहमति होने पर अनुदान प्रदान करेगा।
- केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को निधियाँ देने हेतु जिम्मेदार होगा।
- केंद्र की जिम्मेदारी – पाठ्यचर्या की रुपरेखा बनाना, ट्रेनिंग हेतु मानक बनाना, नवाचार अनुसन्धान योजना क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद एवं संसाधन प्रदान करना।
- धारा 8 – प्रदेश सरकार के दायित्व – 6 से 15 साल के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा देना, जरुरी एडमिशन, उपस्थिति, प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करना, बच्चों के नज़दीक विद्यालय हो, पिछड़े बच्चों से भेदभाव ना हो, विद्यालय बिल्डिंग, अध्यायक, शिक्षण सामग्री देना, उम्र के अनुसार एडमिशन देना और दूसरे विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाने का प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया देना, शिक्षण ट्रेनिंग सुविधा।
- धारा 9 – क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी।
- धारा 10 – सभी माता-पिता, अभिभावक का दायित्व होगा कि बच्चे का विद्यालय में प्रवेश हो एवं रेगुलर विद्यालय जाए।
- धारा 11 – 3 से 6 साल के विद्यार्थी को शुरूआती शिक्षा हेतु तैयार करना और इनकी देखभाल की व्यवस्था देना।
- धारा 12 – सरकार से स्थापित विद्यालय एडमिशन ले चुके विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करवाएगी। सरकारी मदद पाने वाले और प्राइवेट स्कूल प्राइमरी क्लास के कुल 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा देंगे। निजी विद्यालय में शिक्षा हेतु 25 प्रतिशत छात्रों के लिए सरकार राशि देगी। सभी स्कूल स्थानीय प्राधिकारी को माँगी जा रही सूचना देने के लिए बाध्य होंगे।
- धारा 13 – एडमिशन के लिए कोई शुल्क अथवा परीक्षा नहीं होगी। इसका उल्लंघन होने पर विद्यालय को 10 गुना तक शुल्क देना होगा। पहली बार 25 हजार रुपए और इसके बाद 50 हजार रुपए जुर्माना रहेगा।
- धारा 14 – बच्चे की उम्र को सरकार के प्रमाण-पत्रों से तय किया जायेगा। जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र न होने पर स्कूल एडमिशन से मना नहीं कर सकते है।
- धारा 15 – सरकार की ओर से सत्र की शुरुआत में अथवा इसके बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों को तय तरीके से पढ़ाई पूर्ण की जाएगी।
- धारा 16 – किसी भी छात्र को फेल नहीं करेंगे और न ही विद्यालय से निकालेंगे। कम अंकों से विद्यार्थी को फेल नहीं करना है। साथ ही रेगुलर बच्चा आकर अध्ययन करेगा ही।
- धारा 17 – बच्चे को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, मारपीट एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी नहीं होगा। ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
शिक्षण के प्रावधान
| क्लास | दिन | घण्टे |
| पहली से पाँचवी | 200 | 800 |
| छठी से आठवीं | 220 | 1,000 |
प्रतिदिन शिक्षण प्रावधान
| क्लास | रोज का शिक्षण कार्य (घंटे) |
| प्राथमिक कक्षा (पहली से पाँचवीं) | 4 घण्टे |
| उच्च प्राथमिक कक्षा (छठीं से आठवीं) | साढ़े चार घण्टे |
शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात
- धारा 25 में इसका वर्णन है।
- प्राइमरी क्लास में 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा।
- उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक होना जरुरी।
- यदि प्राथमिक कक्षा में 200 से ज्यादा छात्र हो तो विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 40:1 रहेगा।
विद्यालय एवं घर की दूरी
- प्राइमरी क्लास (1 से 5) के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 1 किमी हो।
- सब-प्राइमरी क्लास (6 से 8) के बच्चों के घर से स्कूल की दूरी 3 किमी हो।
- तीन वर्षों के भीतर हर एक घर के समीप स्कूल की व्यवस्था हो।
साप्ताहिक घण्टे
- एक अध्यापक के लिए कम से कम साप्ताहिक घण्टे 45 होंगे।
समावेशी शिक्षा के मायने एवं तरीके
देश की स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था के विकास से इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि देश की शिक्षा ने विविधता होने पर भी एक समावेशी शिक्षा उपकरण की तरह से काम किया है।
समावेशी शिक्षा प्रणाली में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, जोकि हर समुदाय के बच्चे को बिना भेदभाव के शिक्षित होने का बराबर मौका देती है।
- ऐसी शिक्षा हर छात्र के लिए ऊँची एवं सही आशा सहित उसकी व्यक्तिगत शक्तियों को विकसित करती है।
- यह दूसरे छात्रों को अपने समान आयु के बच्चों के साथ में कक्षा गतिविधियों में सहभागिता करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों के ऊपर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- दूसरे बच्चे अपनी निजी ज़रूरतों और क्षमताओं के साथ हर एक का एक विस्तृत विविधता सहित मित्रता को विकसित करने की क्षमता बढ़ती है।
- बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एवं उनके स्कूल की गति विधि में माता-पिता को सम्मिलित करने का पक्षधर है।
आरटीई एक्ट 2009 अधिनियम से जुड़े प्रश्न
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है ?
4 अगस्त 2009 के दिन देश की संसद में यह अधिनियम पारित हुआ है, जिसके अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
आरटीई एक्ट 2009 में अनुच्छेद क्या है ?
RTE Act 2009 में कुल 7 अनुच्छेद है –
प्रारंभिक, बच्चे की शिक्षा का अधिकार, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता-पिता के कर्तव्य, विद्यालय और अध्यापक के काम कर्तव्य एवं अधिकार, शुरूआती शिक्षा और पाठ्यक्रम, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण, विस्तार।
शिक्षा का अधिकार क्या है ?
सरकार द्वारा निःशुल्क शुरूआती शिक्षा देने एवं ‘अनिवार्य’ प्रवेश तय करने का दायित्व है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्य क्या है ?
यह अधिनियम भारत के हर एक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। लाभार्थी बच्चा किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय अथवा समाज से सम्बंधित हो सकता है।
RTE act 2009 ke antargat aane ke liye bachche ke pariwar/mata/pita ki adhikatam warshik incom kitani honi chahiye, please batayen
Respected Sir/Madam,
Please share updated RTE ACT, along with all amendments and modifications/rectifications if any and oblige.
With Thanks and Regards-
Pratap Singh Dhama
Respected Sir/Madam,
Please share, updated RTE ACT- 2009, along with NEP 2020 including all amendments and modifications/ rectifications till date (if any) in special reference/ specilly pertaining to Primary Education.
I’ll be highly obliged.
With Thanks and Regards-
Pratap Singh Dhama
Principal
Edn. Dept.- MCD, GNCT Delhi.