हिंदी भाषा को देश के लगभग 80 करोड़ लोग बोलते है, किन्तु हिंदी शब्द का अर्थ भी बहुत सी मान्यताएँ संजोए हुए है। भाषा एक प्रकार का उच्चारण ध्वनि संकेत होती है। भाषा से मानव अपने विचार एवं शब्द अन्य व्यक्ति तक पहुँचा सकता है। भारत में हिंदी, हिन्दू एवं हिन्दुस्तान आदि शब्दों की उत्पति फारसी भाषा से ही हुई है।
इस लेख में हिंदी शब्द के अर्थ, इतिहास, उत्पत्ति और इसके कठिन शब्द की भी जानकारी दी जाएगी। समय के साथ बहुत सी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में काफी कठिन शब्द आ चुके है।
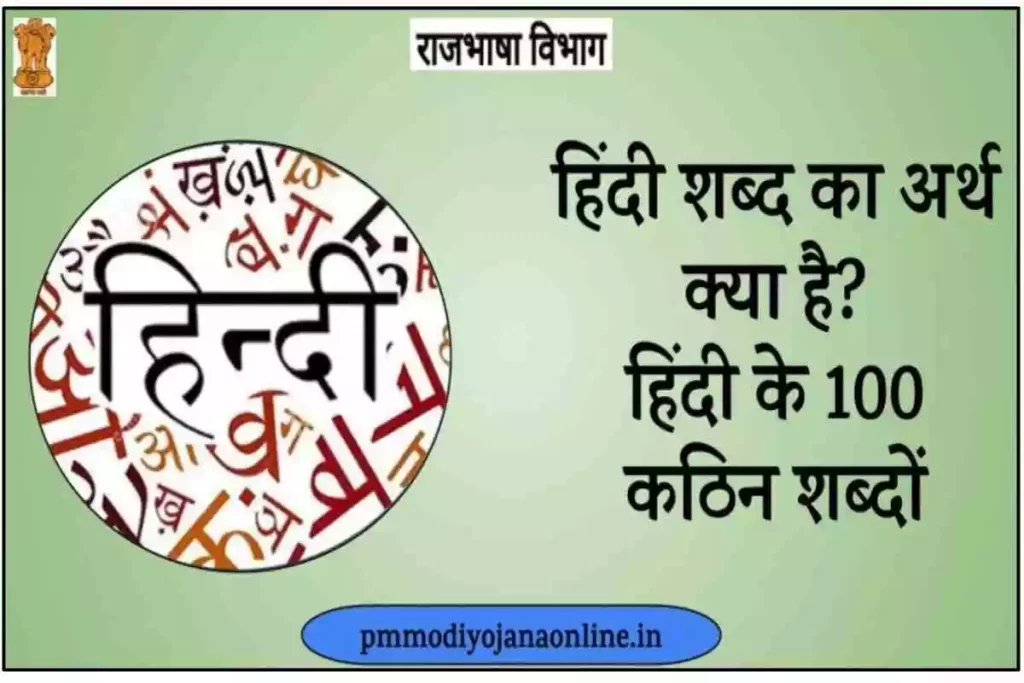
हिंदी शब्द का अर्थ
13वी सदी के मशहूर कवि औफी ने सबसे पहले “हिंदवी” शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब “हिन्दुस्तान की भाषा” है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि ने भी 16वी सदी में ‘हिंदवी’ शब्द का प्रयोग किया। साहित्य एवं लेखों में 17वी शताब्दी से हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है।
18वी सदी में अंग्रेज़ों के अधिकारियों ने भी भारत में हिंदी भाषी लोगों को ‘हिन्दुस्तानी’ नाम दिया था। कुछ जानकारों के अनुसार हिन्दुओं द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया था।
देश की सांस्कृतिक एकता, सामाजिक चेतना एवं आपसी बंधुता को बनाये रखने में हिंदी हमेशा अहम भूमिका निभाती है। हिंदी भाषा के ज्ञान को लेखन आदि में अच्छे से प्रयोग कर सकते है।
हिंदी शब्द का अर्थ की जानकारी
| लेख का विषय | हिंदी शब्द का अर्थ |
| उद्देश्य | हिंदी के कठिन शब्द बताना |
| लाभार्थी | सभी लोग |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://rajbhasha.gov.in/ |
हिंदी के 100 कठिन शब्द
| अर्थवान | मतलब के साथ | विपणन | विक्रय या व्यापार |
| अवगत | जानकारी देना | वितरण | बांटना |
| उजागार | प्रकट, प्रकाशित, सामने आना | दोहन | शोषण करना या लूटपाट |
| अखण्डता | खंडित न होनेवाला या नहीं बटने वाला | अवरूद्ध | रुकावट या बाधा |
| आपूर्ति | भरना या देना | सहभागी | भागीदार या हिस्सेदार |
| अभियान | दल बल सहित चल पड़ना या सैनिक आक्रमण, चढ़ाई | अट्टालिका | किसी ऊँची इमारत का ऊपरी कक्ष या हिस्सा |
| श्रमजीवी | मेहनत से जीविका चलानेवाला | जिजीविषा | जीवित रहने की इच्छा। |
| संवाहक | ले जानेवाला या माध्यम | तारतम्य | किसी घटना या क्रम की आवृत्ति |
| प्रजाति | जीव का एक प्रकार | अक्षुण्ण | जिसके टुकड़े न हो सके |
| निर्वाह | निबाहना | ज्ञापन | जताना या प्रकट करना |
| पुख्ता | पक्का या मजबूत | उपागम | पास आना या घटित होना |
| संवर्ग | अपनी ओर समेटना या अपने लिए बटोरना | समन्वय | नियमित क्रम या संयोग |
| फीसदी | प्रतिशत या प्रति सैकड़ा | भूमिगत | भूमि के अंदर छिपा हुआ |
| व्यापक | विस्तृत या चारों ओर फैला हुआ | श्लाघ्य | प्रशंसनीय |
| त्वरित | तेज़ी से | स्वैराचार | स्वेच्छाचार |
| समीक्षा | छानबीन या जाँच-पड़ताल करना | सुमुत्सुक | उत्साहित |
| मानदेय | किसी कार्य या सेवा के लिए दिया जाने वाला धन | वात्याचक्र | भंवर |
| निजात | छुटकारा पाना | आभास | अहसास |
| अंकक्षेण | बही खातों की जाँच | कंगाल | जिसके पास बिल्कुल धन न हो |
| प्रावधान | नियम या कानून या व्यवस्था | तरणि | नौका |
| प्रायोजन | किसी उत्पाद के प्रचार हेतु कार्यक्रम | अनिष्ट | गलत |
| प्रायोजक | कार्य करने वाला | अवधि | समय सीमा |
| अहमियत | महत्व या गंभीरता | दैव | भाग्य |
| निस्तारण | समाधान करना | अश्लील | गंदा |
| निवारण | रोकने या दूर करने की क्रिया या अवस्था | अनायास | गैरजरुरी |
| वरीयता | रैंकिंग या श्रेष्ठता | अभियान | उद्देश्यपूर्ण यात्रा |
| अवसंरचना | मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना | बीड़ा | ज़िम्मेदारी या भार लेना |
| चेतावनी | आगाह या धमकी | पंजीकरण | नाम लिखवाना |
| संसाधन | कार्य में सहायक सामग्री | निष्पादित | नियम, आदेश निकलना |
| सघन | घना या ठोस | संप्रषेण | भेजना या पहुँचाना |
| वृष्टि | आकाश से जल गिरना या वर्षा या बारिश | विमर्श | विचार, वार्तालाप |
| भागीदारी | हिस्सेदारी | हितग्राहियों | लाभार्थी या ग्रैच्युटी |
| विसर्जित | त्यागा हुआ या बहाया गया | आधारभूत | मौलिक या आधारिक |
| सुमेलित | सही प्रकार से मिलता जुलता | चुनिंदा | चुना हुआ या श्रेष्ठ या उत्तम |
| भयावह | डरावना या भयानक स्थिति | निगरानी | देख-भाल या चुकीदारी |
| आंकड़ा | संख्या | आरूझाई | उलझाना |
| प्रविष्ट | अंदर आया या घुसा हुआ | पाषाण कोर्त्तक | पत्थर की मूर्ति बनाने वाला |
| पारदर्शिता | वस्तु के आर-पार देखेने का गुण या क्षमता | निर्निमेष | अपलक देखना |
| स्वावलम्बी | अपने ही सहारे पर रहने वाला | चरायंध | दुर्गंध |
| जबाबदेही | उत्तरदायित्व या जिम्मेदार | सांसोच्छेदन | सांसों को समाप्त करना |
| विविरणात्मक | विवरण से सम्बन्ध रखने वाला | संगणक | कंप्यूटर |
| हस्तामलकवत् | हथेली पर रखे आंवले के समान | नश्वारता | नाशवान |
| भक्ष्याभक्ष | खादय, अखादय | यत्किंचित | थोड़ा बहुत |
| विस्थापन | लोगों को अपने घरों एवं जमीनों से हटाना | प्रगल्भ | चतुर, हाेशियार |
| गाद | नदियों द्वारा वहन किये जाने वाले मिट्टी, रेत, धूल एवं पत्थर | क्षीणवपु | कमजोर |
| स्वैच्छिक संस्था | एक संस्था जो सरकार से स्वतंत्र हो | सम्बल | सहारा या सहायक |
| प्रावधान | नियम | अस्थि | हड्डी |
| कृतघ्न | उपकार ना मानने वाला | अनुचित | बुरा |
| निर्वाण | मुक्ति, मोक्ष या मृत्यु | रिक्त | खाली |
| निर्माण | बनना | इतिश्री | समाप्ति, अंत या पूर्णता |
हिंदी शब्द की उत्पत्ति
हिंदी शब्द का मूल ‘फारसी’ भाषा में माना जाता है, हिंदी के इतिहास को देखे तो मध्य युग में तुर्किस्तान और ईरान के कुछ मुस्लिम व्यापारी एवं लुटेरे भारत आये थे। उनके लिए भारत सिंधु नदी के पार स्थित था, अतः बोलचाल में वे हिन्दू शब्द का प्रयोग करने लगे। इसी कारण से भारत में बोले जाने वाली भाषा को हिंदी कहा जाने लगा, ऐसे ही यहाँ की भाषा को “हिंदी” पुकारा जाने लगा।
परन्तु कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी विद्वान हिंदी भाषा में ही इसका नामकरण बताते है। जैसे : हिन – हनन करने वाला + दु – दुष्ट, यानि कि दुष्टों का हनन करने वाला।
कुछ के अनुसार हिंदी उन लोगों की भाषा है, जो हीन (हीनों) + दु (दुलन) = हिन्दू अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिन्दू है, और उसकी भाषा हिंदी है।
चूँकि इन व्याख्याओं के प्रमाण कम एवं अनुमान अधिक है, अतः इन्हे सामान्यता अस्वीकार किया जाता है। ऐसे यूनानी के ‘इंडिका’ एवं अंग्रेजी के ‘इंडिया’ शब्द को भी “हिंदीका” शब्द का विकसित रूप कहते है। पहली व्याख्या को मानते हुए हिंदी को संस्कृत भाषा के “सिंध” शब्द से बहुतायत में स्वीकारा जाता है।
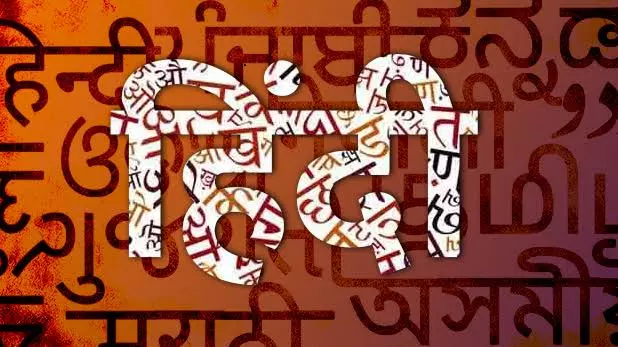
हिंदी शब्द का अर्थ से जुड़े प्रश्न
हिंदी भाषा में कितने शब्द है?
हिंदी में वर्तमान समय तक शब्दों की संख्या 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गयी है।
हिंदी भाषा के तीन अर्थ कौन से है?
आज हिंदी भाषा में तीन अर्थ – व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ एवं विशिष्ट अर्थ मिलते है।
हिंदी में कितने स्वर है?
हिंदी भाषा में उच्चारण के लिए 52 वर्ण है, जिनमे से 41 व्यंजन एवं 11 स्वर है।
हिंदी कौन -सी भाषा का शब्द है?
हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। चूँकि सिंधु नदी के सिंध का ईरानी भाषा में हिन्द उच्चारण हुआ।